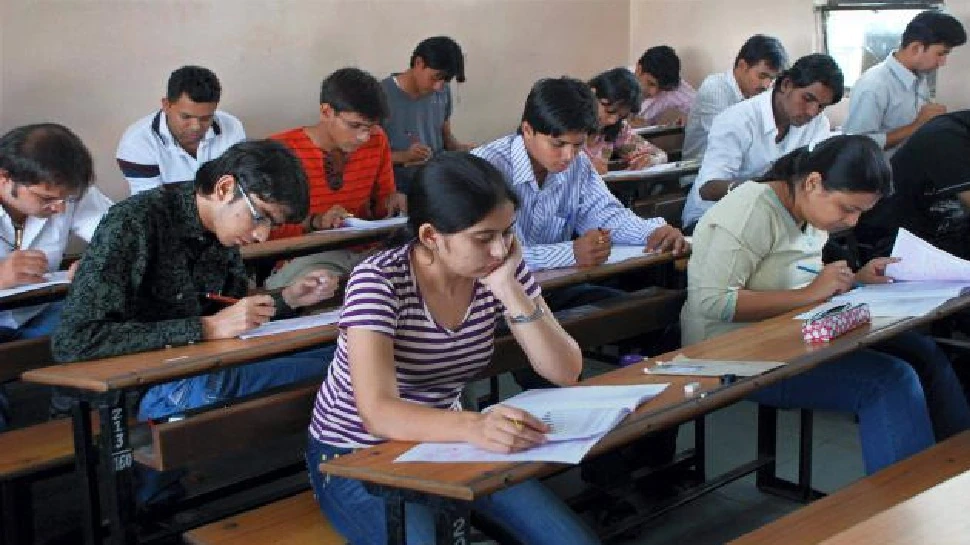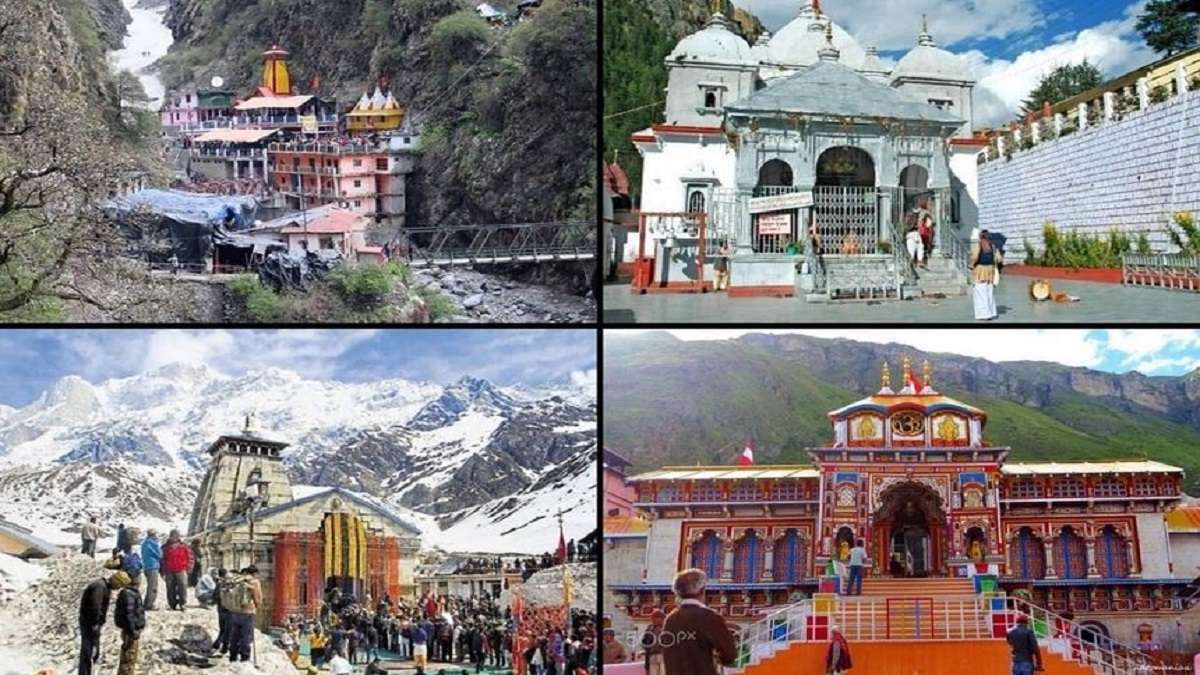उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के विलय के फैसले को लेकर विरोध-प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार, 14 जुलाई को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। वहीं, मंगलवार 15 जुलाई को अपना दल (कमेरावादी) की अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जोरदार प्रदर्शन किया। नावेल्टी चौराहे से विधानसभा की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका, जिससे मौके पर जमकर नोकझोंक भी हुई।
पल्लवी पटेल ने इस दौरान सरकार पर “तानाशाही रवैये” का आरोप लगाया और कहा कि जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। उनका कहना है कि स्कूलों का विलय गरीबों और वंचित वर्गों के बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीनने जैसा है।
सरकार की नीति पर सवाल, शिक्षा व्यवस्था पर चोट का आरोप
पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया कि यह पूरी प्रक्रिया योजनाबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। पहले सरकारी संस्थानों में भर्तियों पर रोक लगाई गई, फिर निजीकरण की नीति को आगे बढ़ाया गया और अब परिषदीय स्कूलों को बंद कर शिक्षा के अधिकार पर सीधा हमला किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार 27,746 प्राथमिक स्कूलों को बंद करने जा रही है, जो ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। इन स्कूलों में गरीब, पिछड़े और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में इन स्कूलों को बंद करना संविधान में दिए गए “शिक्षा के अधिकार” (Right to Education) के खिलाफ है।
सरकार की सफाई – संसाधनों का बेहतर उपयोग ही मकसद
दूसरी ओर सरकार का कहना है कि स्कूलों का “पेयरिंग” यानी विलय, संसाधनों के समुचित उपयोग और बच्चों के हित में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन स्कूलों में 50 से अधिक विद्यार्थी हैं, उन्हें बंद न किया जाए। सरकार की योजना के अनुसार, जिन स्कूलों में छात्र संख्या बहुत कम है, उन्हें नजदीकी बड़े स्कूलों के साथ जोड़ा जाएगा ताकि बच्चों को बेहतर सुविधा, शिक्षक और संसाधन मिल सकें। इसके अलावा, जो स्कूल बंद किए जाएंगे, वहां आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की योजना है ताकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की देखभाल व पोषण से जुड़े कार्यक्रम जारी रह सकें।
शिक्षा पर सियासत या जमीनी हकीकत?
विपक्ष का तर्क है कि स्कूलों का विलय ग्रामीण और गरीब बच्चों की शिक्षा के अधिकार को प्रभावित करेगा। वे इसे शिक्षा के निजीकरण की ओर एक और कदम बता रहे हैं। वहीं, सरकार इसे “शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने” का एक उपाय बता रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या यह फैसला ज़मीनी सच्चाई को ध्यान में रखकर लिया गया है, या फिर यह केवल आंकड़ों और बजट के संतुलन की कवायद है? विपक्ष सरकार से यह मांग कर रहा है कि पहले स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक, बुनियादी सुविधाएं और संसाधन मुहैया कराए जाएं, उसके बाद किसी तरह के विलय पर विचार हो।