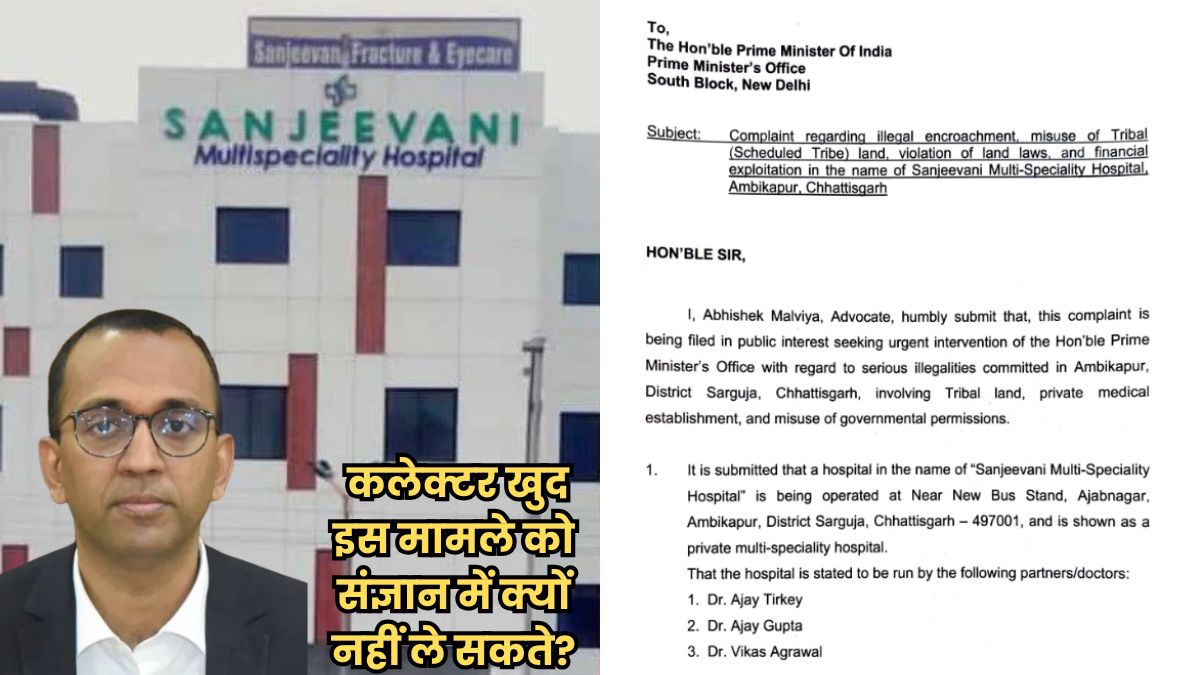अजय बोकिल
यह संभवत: पहली बार है, जब देश की सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी वाले राज्य मध्यप्रदेश में आदिवासियों को लुभाने के लिए इस कदर राजनीतिक खींचतान मची है। जहां सत्तारूढ़ भाजपा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को राजधानी भोपाल में ‘जनजातीय गौरव दिवस’ मना रही है, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सम्बोधित करेंगे, वहीं विपक्षी कांग्रेस ने इस दिन जबलपुर में जनजातीय सम्मेलन करने का ऐलान किया है़, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शामिल होंगे।
इसके पहले मप्र में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा स्वायत्तता देने वाला पेसा कानून लागू करने की घोषणा की। यह कानून देश के 10 राज्यों में लागू है। यह बात अलग है कि ज्यादातर राज्यों में इसे आधे-अधूरे ढंग से ही लागू किया गया है। कई राज्यों में तो इसके नियम ही नहीं बने हैं और जहां बने हैं, वहां पालन कितना हो रहा है, यह स्वतंत्र अध्ययन का विषय है।
ये भी पढ़े – Indore News : जीजा पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को आजाद नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया
जहां तक मध्यप्रदेश की बात है तो ‘पेसा कानून’ नया राजनीतिक दांव है। यह भी कम हैरानी की बात नहीं है कि आदिवासियों को ज्यादा अधिकार देने वाला जो कानून संसद ने 1996 में पारित किया हो, उसे देश की सर्वाधिक आदिवासी आबादी वाले राज्य में लागू होने में 25 साल लग गए (अभी यह घोषणा ही है), जबकि इस दौरान कांग्रेस आठ साल सत्ता में रही और भाजपा 15 साल से है। इस बीच ऐसा क्या हुआ है, जो भाजपा और कांग्रेस में अचानक आदिवासी प्रेम उमड़ आया है, जबकि आदिवासी वही हैं, उनकी आर्थिक-सामाजिक हालत और समस्याएं भी कमोबेश वही हैं।
शिक्षा और सस्ते राशन के बाद भी मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा भुखमरी और कुपोषण के शिकार आदिवासी ही हैं। मध्यप्रदेश में आदिवासियों की आबादी डेढ़ करोड़ से ज्यादा है। इनमें भी एक ितहाई भील और इससे कुछ कम आबादी गोंड आदिवासियों की है। वैसे राज्य में 43 से ज्यादा आदिवासी जनजातियां हैं, लेकिन इनमें भी 6 जनजातियां कुल आदिवासी आबादी का 92 फीसदी हैं। जिन बिरसा मुंडा की स्मृति में यह महाआयोजन हो रहा है, उस मुंडा समुदाय की मप्र में जनसंख्या केवल 5 हजार है।
कुल की करीब 22 फीसदी आबादी होने से मप्र में 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। दरअसल सारा खेल इन्हीं सीटों पर काबिज होने का है। 2003 के पहले तक मप्र की अधिकांश आदिवासी सीटों पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा। कुछ अपवाद छोड़ दे तो इसका बड़ा कारण कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पार्टी की आदिवासियों तक ज्यादा पहुंच ही नहीं थी। बीच में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसे दलों ने गोंड इलाकों में जरूर कुछ जोर मारा दिखाया। यूं भी राज्य में सभी आदिवासी समुदाय भाषा, रहन-सहन, संस्कृति,परंपरा और भौगोलिक हिसाब से बंटे हुए हैं।
केवल आदिवासी होना ही उनके बीच समान सूत्र है। आदिवासियो के बढ़ते धर्मांतरण के बीच बीते तीन दशको से आरएसएस और भाजपा ने आदिवासी इलाकों में अपनी पैठ बनाई है। जिसका नतीजा रहा कि 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 47 आदिवासी सीटों में से 31 सीटे जीतने में कामयाब रही। आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियो की सक्रियता के मद्देनजर संघ ने आदिवासियों को हिंदुत्व से जोड़ने की पुरजोर कोशिश की है। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 25 आदिवासी सीटें गंवा दीं और ये ज्यादातर कांग्रेस ने जीत लीं।
संदेश गया कि आदिवासी इलाकों में कांग्रेस की पैठ ज्यादा गहरी है, बजाए भाजपा के। अब चुनौती दोनो दलों के सामने है। भाजपा के समक्ष चुनौती यह है कि वह आदिवासी वोट बैंक को अपने भरोसेमंद वोट के रूप में कैसे तब्दील करे, जबकि कांग्रेस के सामने सवाल यह है कि वो भाजपा की आक्रामक रणनीति के चलते अपने परंपरागत आदिवासी वोट बैंक को कैसे बचाए रखे। आदिवासी क्षेत्रों में विकास के सरकारी दावे अपनी जगह हैं, लेकिन आदिवासियों को समुचित राजनीतिक महत्व न तो भाजपा ने दिया और न ही कांग्रेस ने। वो निर्णायक भूमिका में कहीं भी नहीं हैं।
आदिवासी हितैषी होने का राग अलापती रही कांग्रेस ने तो दो मौको पर राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री बनने की संभावना पर भी चतुराई से पानी फेर दिया, जबकि भाजपा ने तो ऐसी नौबत ही नहीं आने दी। यानी दोनो को आदिवासियों का साथ तो चाहिए मगर अपनी शर्तों और राजनीतिक सुविधा के साथ। यह चालाकी अब आदिवासियों की भी समझ में आने लगी है। खासकर शिक्षित आदिवासियों में। यही कारण है कि आदिवासी पहचान को लेकर संघर्ष करने वाले संगठन ‘जय आदिवासी युवा संगठन’ का जन्म हुआ।
हालांकि इसका असर अभी मुख्य रूप से मालवा के कुछ भील आदिवासी इलाको में ही है, लेकिन स्थापित राजनीतिक दल इससे खतरा महसूस करने लगे हैं। ‘जयस’ की राजनीतिक दिशा, रणनीति और प्रतिबद्धता यदि सही रहती है तो भविष्य में यह बड़ी राजनीतिक ताकत बन सकता है। माना जाता है कि ‘जयस’ को खड़ा करने में भी कांग्रेस का ही हाथ है। कुलमिलाकर यह धारणा मजबूत हो रही है कि मध्यप्रदेश में सत्ता की चाभी अब आदिवासी वोट बैंक के हाथ में रहने वाली है। ये वोट बैंक जिधर झुकेगा, सत्ता सिंहासन उसी को मिलेगा।
मसलन 2018 के विधानसभा चुनाव में यदि भाजपा कुल आदिवासी सीटों में से आधी भी जीत पाती तो चौथी बार सीधे सत्ता में लौटती। उधर कांग्रेस की कोशिश है कि आदिवासी सीटों पर उसका दबदबा पहले की तरह कायम रहे। हालांकि आदिवासी कल्याण अथवा उनके राजनीतिक प्रमोशन का कोई ठोस कार्यक्रम कांग्रेस के पास दिखाई नहीं देता। साथ ही उसे ‘जयस’ के भस्मासुर साबित होने का भी डर है।
यूं महान आदिवासी सेनानी बिरसा मुंडा के प्रति हाल में भाजपा में जागी भक्ति का एक बड़ा कारण यह भी है कि बिरसा मुंडा ने 19 वीं सदी के अंत में आदिवासियों के जंगल, जमीन और अधिकारों के लिए अंगरेजों से तो लड़ाई लड़ी ही, साथ में ईसाई मिशनरियों को भी खुली चुनौती दी थी। खास बात यह है कि बिरसा ने आधुनिक शिक्षा ईसाई मिशनरी में ही हासिल की थी और ईसाई धर्म भी स्वीकार कर लिया था।
लेकिन बाद में उन्हें आत्मज्ञान हुआ और ईसाई धर्म त्याग कर वो अपने मूल आदिवासी धर्म में लौटे तथा अन्य आदिवासियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। इससे बिरसा मुंडा की ख्याति स्वतंत्रता सेनानी के साथ-साथ एक संत के रूप में भी होने लगी। बहरहाल मध्यप्रदेश में राजनीतिक दलों का ध्यान आदिवासियों के आराध्य, प्रतीकों, अधिकारों और सियासी रूझान पर है।
मप्र में पेसा (अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार) कानून लागू होने के बाद आदिवासियों को कितनी ताकत मिलेगी, यह तो बाद में पता चलेगा। हो सकता है इससे आदिवासियों की राजनीतिक चेतना और मुखर हो, आत्मविश्वास बढ़े। क्योंकि वन संरक्षण, वन क्षेत्रों में खनन की अनुमति सहित कई अधिकार आदिवासी ग्राम सभाअोंको इसे कानून के तहत मिलेंगे। इसी के साथ भ्रष्टाचार के नए आयाम भी हमे देखने को िमल सकते हैं।
फिलहाल भाजपा की कोशिश यही है कि वह राज्य में आदिवासियों का खोया समर्थन फिर कैसे हासिल करे। इसी संदर्भ में हाल के उपचुनाव में जोबट आदिवासी सीट भाजपा द्वारा कांग्रेस से छीन लेने का प्रतीकात्मक महत्व ज्यादा है। उप चुनाव के पहले कांग्रेस ने ‘आदिवासी अधिकार’ यात्रा भी निकाली थी। लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिला।
इसीलिए राजनीतिक हल्को में भीलों के आदर्श ट्ंट्या भील, गोंड राजा शंकरशाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, शहीद बिरसा मुंडा आदि को शिद्दत से याद किया जा रहा है। पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने तो ‘विश्व आदिवासी दिवस’ पर 9 अगस्त (यह अगस्त क्रांति दिवस भी है) को राज्य में सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी थी। भाजपा सरकार ने उसे हटा दिया, लेकिन बिरसा मुंडा जयंती की छुट्टी घोषित कर दी।
बहरहाल प्रतीकों की इस राजनीति से ‘जनजातीय गौरव’ कैसे लौटेगा यह तो समय के साथ पता चलेगा। क्योंकि ‘गौरव’ से भी ज्यादा आदिवासियों की असली समस्या उनकी अपनी मूल पहचान कायम रखने, भूख, अशिक्षा, बेरोजगारी और उनके मूल निवास जंगलों के खत्म होते जाने और शहरी संस्कृति में वाजिब सम्मान हासिल करने की है। इससे भी बड़ी कसक उनके राजनीतिक असर को लेकर है।
आदिवासी बदलते वक्त के साथ शहरी सभ्यता के साथ कदम ताल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में महाभारत काल के ‘एकलव्य’ वाली स्थिति बहुत ज्यादा नहीं बदली है। दूसरी तरफ धर्मांतरण ने आदिवासियों के भीतर ही एक नई दीवार उठा दी है। वो असमंजस में हैं कि खुद को भारतीय माने कि हिंदू मानें, ईसाई या मुसलमान मानें? या सिर्फ आदिवासी मानें?