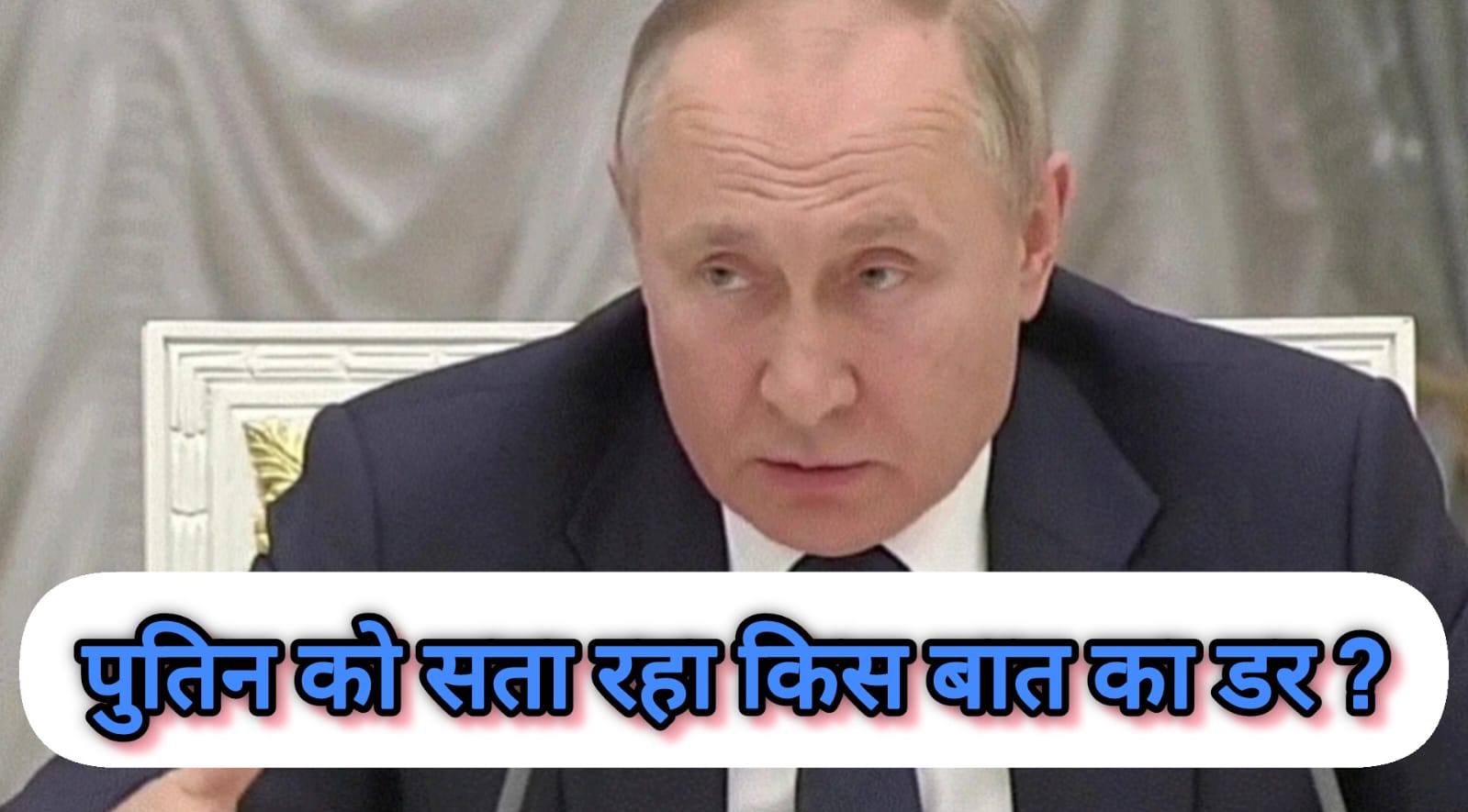अजय बोकिल
पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बैनर्जी की धमाकेदार जीत, असम में भाजपा और केरल में वाम गठबंधन की वापसी, यूपी पंचायत चुनाव में भाजपा की सिकुड़ती ताकत, बंगाल में चुनाव पश्चात हिंसा और श्मशान में शहनाई की तरह बजते आईपीएल की दुकान बंद होने जैसे कई घटनाएं हाल में घटी हैं, िजन पर लिखे जाने की अपेक्षा कई मित्रों को थीं। लेकिन लगा कि कोरोना का महाभयंकर शिकंजा इन सब पर भारी है। आपदाएं आती हैं, बड़े हादसे भी होते हैं, लेकिन मौत का ऐसा चौतरफा मंजर सचमुच अकल्पनीय है। ऐसा मंजर जो व्यक्ति, समुदाय और सम्प्रदाय िनरपेक्ष है।
जिसके निरंकुश तांडव में हमारी लाचारियों और मूर्खताअोंके कर्कश घुंघरू भी बज रहे हैं। आलम यह है कि कब आपका कौन-सा हंसता-बोलता परिचित या परिजन अचानक घुटती सांसों के बीच दम तोड़ देगा, कल्पना करना भी मुश्किल है। अब दिन की शुरूआत ही किसी न किसी के चल बसने की खबर से होती है। एक के दिवंगत होने की खबर का झटका मंद भी नहीं पड़ता कि किसी दूसरे के जाने का सदमा झकझोर देता है। कहां तक गिनती करें। एक को श्रद्धांजलि देकर मन कुछ हल्का होता है तो किसी दूसरे के बिछुड़ने के गम में सांत्वना के नए शब्दों की तलाश शुरू करनी पड़ती है। उफ्, ये असमाप्त श्रद्धांजलियों का दौर कब थमेगा?
जिस कदर कोरोना वायरस इस देश में कहर ढा रहा है, उसमें सरकार, व्यवस्था और समाज तो दोषी हैं ही, वो ईश्वर भी कहीं जिम्मेदार है, जो लाखों-कराहों को अनसुना किए बैठा है। हादसे में मौतें तो सुनी थीं, लेकिन एक अदृश्य वायरस कुछ ही घंटों में परिवार के परिवार के लील जाएगा, यह सूचना भी भीतर से कंपा देती है। यानी एक के जीने की आस बंधती है तो दूसरा दुनिया से उठ जाता है। हम यह सब होते देख रहे हैं, उसे रोकने की हैसियतभर कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन लगता है काल के हाथ हमारे हाथों से कई गुना लंबे और निष्ठुर हैं।
वो समय शायद गया, जब अंतिम यात्रा या अंत्येष्टि भी जीवन का आखिरी लेकिन अनिवार्य संस्कार होती थी। ‘श्मशान वैराग्य’ के साथ ही सही, लोग अपनों को आखिरी विदाई के लिए एकत्र होते थे। सच्चे या अधूरे मन से ही सही दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए दो शब्द कहते थे। दो मिनट का मौन रखते थे। शोकाकुल परिवार को ‘सब ठीक होगा’ कहकर हिम्मत बंधाते थे। यह जानते हुए भी दुनिया उसी जीवटता से और उसी कुटिलता के आगे बढ़ती रहेगी। कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ‘श्मशान वैराग्य’ मैंने इसलिए कहा कि श्मशान घाट में मृतक को अंतिम विदाई देते समय चिता से उठते धुएं या कब्रिस्तान में एक मुट्ठी खाक डालते वक्त क्षणभर के लिए ही जीवन की क्षण भंगुरता का अहसास भीतर तक होता है। यानी एक ‘खेला’ है, जो आदमी अपने तयशुदा किरदार के हिसाब से खेलकर किसी और दुनिया में चल देता है। तब लगता है कि ऐसा जीना भी क्या जीना..! लेकिन मनुष्य है कि यह भाव वह अगले ही क्षण झटक कर नई चुनौतियों से जूझने के लिए सन्नद्ध हो उठता है। क्योंकि जीवन चलने का नाम है। श्मशान भूमि पर उपजा क्षणिक वैराग्य विश्राम घाट से निर्गम होते ही हवा के झोंके में विलीन हो जाता है।
लेकिन कोरोना-संहार का ‘उपसंहार’ शायद ऐसा नहीं है। आप न तो किसी को विधिवत अंतिम विदाई दे सकते हैं और न ही किसी के आंसू पोंछ सकते हैं। अंत्येष्टियां अब केवल मुर्दे को जलाने या गाड़ने के मैकेनिकल कर्मकांड तक सिमट गई हैं। मौत की रस्म अदायगी भी मौत को आमंत्रण का बायस बन गई है। सच तो यह है कि कई घरों में कुछ ही घंटों में इतनी मौतें हो चुकी हैं कि रोने के लिए आंसू भी सूख चुके हैं। पड़ोसियों में भी इतना साहस नहीं बचा कि वो ढाढस बंधा सकें। अर्थियां और जनाजे देखकर ज्यादातर ( कुछ देवदूतों को छोड़ दें तो) लोग मुंह फेर लेते हैं कि कहीं कोरोना उस मातमी हवा पर सवार होकर उन्हें न डस ले।
सबसे अफसोसनाक बात तो यह हुई है कि अब श्रद्धांजलियां भी खेमों में बंट गई हैं। यानी अपने खेमे या गुट का हुआ तो ‘श्रद्धांजलि’ वरना ‘गरियांजलि।‘ इस वैचारिक दुराग्रह ने मानो मनुष्यता का ही कफन तार-तार कर दिया है। कोई व्यक्ति मरने के बाद उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, किस नीयत से कहा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, किस भाव से लिखा जा रहा है, यह जानने की स्थिति में होता है या नहीं, कह नहीं सकते। लेकिन आज देश और समाज इस बुरी तरह बंट चुका है कि मौत का औचित्य भी ‘मेरे-तेरे’ के हिसाब से तय हो रहा है। अभी तक यह सामाजिक मर्यादा अमूमन रहती आई थी कि कम से कम मृत्यु के बाद दिवंगत की सराहना भले न करें, लेकिन उसे गरियाएं तो नहीं। इसलिए भी क्योंकि इंसान अच्छा हो या बुरा, अपना हो या पराया, समर्थक खेमे का हो या विरोधी खेमे का, था तो इंसान ही। मनुष्यता का तकाजा है कि उसके जाने के बाद तो उसे अपशब्द तो न कहें। कोरोना काल में यह अघोषित मर्यादा भी हम पूरी बेशरमी के साथ टूटते हुए देख रहे हैं। यह स्थिति तब है, जब कोरोना से ज्यादातर ‘अच्छे’ लोग ही दुनिया से विदा हो रहे हैं। इस फानी दुनिया से जाने वाले को उसके जाने के बाद जिंदा समाज क्या कहता है, सोचता है, इससे शायद ही कोई फर्क पड़ता होगा, लेकिन उस दिवंगत के प्रति हम अपने मन की भड़ास निकाल कर खुद को अपनी ही नजर में गिराने की निकृष्ट प्रतिस्पर्द्धा में जरूर शामिल हो रहे हैं। मौत का अफसोस मनाने की जगह कुछ लोग उसके औचित्य के तर्क ढूंढने और उसे स्थापित करने का निहायत घटिया काम करने में जुटे हुए हैं। इसे क्या कहें ?
शायद इसी एकांगी सोच का नतीजा है कि अब श्रद्धांजलियां भी एकांगी होती जा रही हैं। हमारा मरे तो दिवंगत, दूसरे का मरे तो मुआ निपटा ! अपने की मृत्यु पर शोक तो गैर की मौत पर बेशर्म जश्न ! यह कैसी संवेदना है, जिसमे वेदना का अंशमात्र नहीं है।
इससे भी क्षुब्ध करने वाली बात श्रद्धांजलियों की वह अवांछित श्रृंखला है, जिसका अंत कहां जाकर होगा, कोई नहीं जानता। दुख की अति भी शायद करूणा का कत्ल कर देती है। ‘कफन’ की एक कहानी मन को झकझोर देती है, लेकिन ‘कफनों की रैलियां’ ही अगर नजर से गुजरने लगें तो दिल पत्थर होने लगता है। सांत्वना देना, धीरज बंधाना, जीने की हिम्मत देना जैसे शब्द निष्प्राण से लगने लगे हैं। प्राकृतिक आपदा, युद्ध, यदा-कदा महामारी और अकाल के अलावा काल का ऐसा तांडव दुनिया ने कम ही देखा होगा। लेकिन बेरहम कोरोना ने मानो जीवन का व्याकरण ही बदल कर रख दिया है। जन्म के साथ ही मृत्यु का भय भी मन को मथने लगा है। आज ये गया, कल वो गया, अगला कब चल देगा, कह नहीं सकते। कब किस वेंटीलेटर (घटिया होने के कारण भी) पर किस की सांसें थम जाएंगी, कब आॅक्सीजन का टोटा आपकी सांसों पर ब्रेक लगा देगा, कहना मुश्किल है। अस्पतालों पर से भी भरोसा उठ-सा गया है। यानी आप के हाथ में केवल अपनी ‘बारी’ का इंतजार करना भर रह गया है…।
कोरोना स्वयं जितना क्रूर है, उतना ही वह हमारी अव्यवस्थाअोंऔर अदूरदर्शिता पर भी अट्टहास कर रहा है। हमारी आत्मचेतना के खोखलेपन पर कुटिलता के साथ मुस्कुरा रहा है। मानो िचढ़ा रहा है कि देखता हूं और कितनी श्रद्धांजलियां देने की हिम्मत है तुम्हारे पास….! अगर हो तो बताएं…